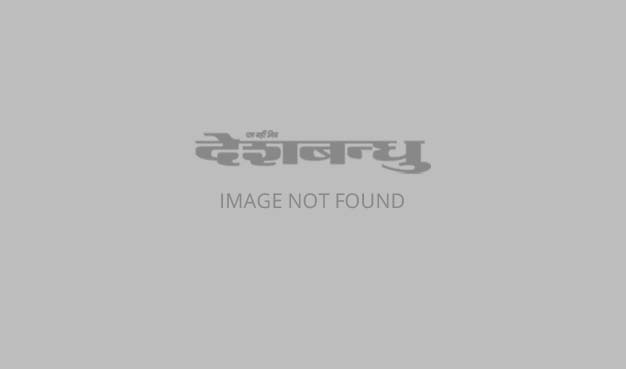
शैलेंद्र चौहान
गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण जरिया बन चला है। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों जहां पीडीएस बड़ा खस्ताहाल हुआ करता था, में भी इसका लाभ हुआ है। यह बात ठीक है कि सामाजिक सुरक्षा के मद में होने वाले खर्च में कुछ अपव्यय होता है जाहिरा तौर पर यह प्रशासनिक- राजनीतिक भ्रष्ट दर्शन है। लेकिन इन दोनों ही मामलों में समाधान पूरी व्यवस्था को खत्म करने में नहीं बल्कि उसे सुधारने में है और इस बात के अनेक साक्ष्य मौजूद हैं कि ऐसा किया जा सकता है।
शायद ही किसी को अब उस चि_ी की याद होगी जो खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर चुनाव के पहले नरेन्द्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखी था। इस चि_ी में मोदी ने दुख जताया था कि खाद्य सुरक्षा का अध्यादेश एक आदमी को दो जून की रोटी भी नहीं देता। खाद्य-सुरक्षा के मामले पर लोकसभा में 27 अगस्त 2013 को बहस हुई तो उसमें भी ऐसे ही उद्गार सामने आए। तब भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इसको ऊँट के मुंह में जीरा डालने की कसरत के माफिक कहा था। अब इन बातों के भुला दिए जाने की एक वजह है इनका सामाजिक नीति विषयक उस गल्प-कथा से मेल न खाना जिसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने गढ़ा था। यह गल्प-पुराण कई भ्रांतियों को समेटकर बना है जैसे- एक, कि राज्यसत्ता के रूप में भारत राजनेताओं की नानी-दादी का घर बनता जा रहा है जो सच तो सभी पार्टियों के लिये है लेकिन निशाना मात्र नेहरू खानदान रहा, क्योंकि इस वक्त कॉँग्रेस के साथ वही सबसे खराब स्थिति में था, 1)बीजेपी नेताओं ने यह जमकर प्रचारित किया (अनेकानेक कारणों से प्रेस खुलकर मोदी लहर की निर्मिति में सहायक थी) कि सामाजिक मद में सरकार दोनों हाथ खोलकर धन लुटा रही है जो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। 2) कि सामाजिक मद में होने वाला खर्च ज्यादातर बर्बाद जाता है - यह एक भीख की तरह है और भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक निकम्मेपन की वजह से गरीब तबके को हासिल नहीं होता। 3) कि इस भारी-भरकम फिजूलखर्ची के पीछे उन पुरातनपंथी नेहरूवादी समाजवादियों का हाथ है जिन्होंने यूपीए शासनकाल में देश को गलत राह पर धकेल दिया। 4) कि मतदाताओं ने इस रवैए को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लोग विकास (ग्रोथ) चाहते हैं, अधिकार नहीं। और, पांचवीं भ्रांति यह कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने इन बेबकूफियों को दुरुस्त करने और लोक-कल्याणकारी राज्य के आभासी कारोबार को समेटने का मन बना लिया है। ये पाँचों दावे बार-बार दोहराए जाने के कारण सच से जान पड़ते हैं लेकिन वे असल में निराधार हैं। अब इन दावों की एक-एक बात कि जाँच की जाये तो लब्बोलुबाब यह कि- कहना कि भारत में सामाजिक मद में किया जाने वाला खर्घ्चा बहुत ज्यादा है तथ्यों से परे तो है ही हास्यास्पद भी है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स (डब्ल्यूडीआई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सबसे कम विकसित देशों के 6.4 प्रतिशत की तुलना में भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा के मद में सरकारी खर्चा जीडीपी का महज 4.7 प्रतिशत, उप-सहारीय अफ्रीकी देशों में 7 प्रतिशत, पूर्वी एशिया के देशों में 7.2 प्रतिशत तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीसीडी) के देशों में 13.3 प्रतिशत है। एशिया डेवलपमेंट बैंक की एशिया में सामाजिक-सुरक्षा पर केंद्रित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत इस मामले में अभी भी बहुत पीछे है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सामाजिक सहायता के मद में जीडीपी का महज 1.7 फीसद हिस्सा खर्घ्च होता है, जबकि एशिया के निम्न आय-वर्ग की श्रेणी में आने वाले देशों में यह आंकड़ा 3.4 प्रतिशत, चीन में 5.4 प्रतिशत और एशिया के उच्च आय-वर्ग वाले देशों में 10.2 प्रतिशत है। जाहिर है, भारत सामाजिक मद में फिजूलखर्ची नहीं बल्कि कमखर्ची में उस्ताद है। सामाजिक मद में होनेवाला खर्च बर्बाद जाता है, इस विचार का भी कोई वस्तुगत आधार नहीं हैं। आर्थिक विकास के लिए लोगों के जीवन में बेहतरी और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की क्या अहमियत है ये आर्थिक शोधों में साबित हो चुका है। केरल से लेकर बांग्लादेश तक, सरकार ने जहां भी स्वास्थ्य के मद में हल्का सा जोर लगाया है वहां मृत्यु-दर और जनन-दर में कमी आई है। भारत के मिड डे मील कार्यक्रम के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं कि इससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, उनके पोषण और तथा पढ़ाई-लिखाई की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। मात्रा में बहुत कम ही सही लेकिन सामाजिक सुरक्षा के मद में दिया जाने वाली पेंशन लाखों विधवाओं, बुजुर्गों और देह से लाचार लोगों की कठिन जिंदगी में मददगार साबित होती है। गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण जरिया बन चला है। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों जहां पीडीएस बड़ा खस्ताहाल हुआ करता था, में भी इसका लाभ हुआ है। यह बात ठीक है कि सामाजिक सुरक्षा के मद में होने वाले खर्च में कुछ अपव्यय होता है जाहिरा तौर पर यह प्रशासनिक- राजनीतिक भ्रष्ट दर्शन है। लेकिन इन दोनों ही मामलों में समाधान पूरी व्यवस्था को खत्म करने में नहीं बल्कि उसे सुधारने में है और इस बात के अनेक साक्ष्य मौजूद हैं कि ऐसा किया जा सकता है।
भारत में सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा के हुए विस्तार से नेहरूवादी समाजवाद का कोई खास लेना-देना नहीं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना स्वाभाविक ही है। बड़े पैमाने पर ऐसा ही विस्तार बीसवीं सदी में सभी औद्योगिक देशों में हुआ था (संयुक्त राज्य अमेरिका आंशिक तौर पर इस प्रक्रिया का अपवाद है)। ऐसा साम्यवादी विचारधारा के देशों में भी हुआ भले ही वजह कुछ और रही। कई विकासशील देश, खासकर लातिनी अमरीका और पूर्वी एशिया के देश हाल के दशकों में ऐसी ही अवस्था से गुजरे हैं। भारत के केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य, जहां वंचित तबके की तनिक राजनीतिक गूंज है, ऐसी ही प्रक्रिया से गुजरे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपीए चुनाव इसलिए हारी क्योंकि मतदाता भिक्षादान के इस कर्मकांड से उकता चुके थे? यह धारणा कई कारणों से असंगत है। एक तो यही कि भिक्षादान इतना था ही नहीं कि उससे उकताहट हो। यूपीए ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत जरूर की लेकिन यह साल 2005 की बात है और इससे यूपीए को बाधा नहीं पहुंची बल्कि 2009 के चुनावों में फायदा ही हुआ। इसके बाद से यूपीए ने सामाजिक क्षेत्र में नीतिगत तौर पर कोई बड़ी पहल नहीं की सिवाय राष्ट्रीय खाद्य-सुरक्षा अधिनियम के जिस पर अमल होना अभी शेष है। साल 2014 के आते-आते यूपीए सरकार के पास अपने पक्ष में कहने के लिए बहुत कम रह गया था। जबकि ऐसी बहुत सारी चीजें थीं जिसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। सोलहवीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों के दौरान मीडिया में तमाम भ्रांतियां बनाई गईं। सामाजिक कल्याण की नीतियों और योजनाओं की आलोचना करते हुए उन्हें देश की खराब विकास दर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। एक भ्रम खड़ा किया गया कि भारत सामाजिक मद में जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहा है। ऐसा प्रचार किया गया कि यूपीए सरकार अपनी इन्हीं सामाजिक कल्याण और अधिकार वाली नीतियों के कारण चुनाव हारी है लेकिन यह तथ्यसंगत नहीं है। यूपीए सरकार में मजबूत हो चुकी कॉरपोरेट लॉबी भाजपा गठबंधन की सरकार में और ज्यादा उत्साहित है। कारोबारी जगत को आम तौर पर गरीबों को दी जाने वाली छूट नागवार गुजरती है। बहरहाल, चुनाव में धन, संगठन और भाषणबाजी, ये तीन चीजें बड़े काम की साबित होती हैं और बीजेपी के पास ये तीन चीजें मौजूद थीं। ऐसे में क्या अचरज है कि हर दस में से तीन मतदाता ने उसे एक मौका देने का फैसला किया? जहां तक पांचवें बिन्दु का सवाल है, इस बात के कोई प्रमाण नहीं कि सामाजिक-कल्याण की योजनाओं को समेटना बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल है। जैसा कि इस आलेख में ऊपर जिक्र आया है, बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रीय खाद्य-सुरक्षा अधिनियम को और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाने की मांग की थी। स्वर्गीय गोपीनीथ मुंडे ने ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार संभालते ही इस अधिनियम को अपना समर्थन जाहिर किया था। सभी बातों के बावजूद ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों के संभावित प्रतिकूल प्रभाव होने के संकेत मिलते हैं। कॉरपोरेट जगत के मन में सामाजिक मद में होने वाले खर्चे को लेकर हमेशा वैरभाव रहता है क्योंकि उसके लिए इसका मतलब होता है ऊँचे टैक्स, ब्याज-दर में बढ़ोत्तरी या फिर व्यवसाय के बढ़ावे के लिए मिलने वाली छूट का कम होना। कारपोरेट लॉबी यूपीए के जमाने में ही प्रभावशाली हो चुकी थी। यह लॉबी अब और भी जोशीले तेवर में है कि सरकार की कमान उनके आदमी यानी नरेन्द्र मोदी के हाथ में है। कारोबार जगत की खघ्बरों से ताल्लुक रखने वाले अखबारों के संपादकीय पर सरसरी निगाह डालने भर से जाहिर हो जाता है कि वे सामाजिक क्षेत्र में भारी सुधार की उम्मीद से भरे हैं।
सामाजिक नीति के कथा-पुराण की वास्तविकता यही है। कहने का आशय यह नहीं कि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक-सुरक्षा के मद में रचनात्मक सुधार की जरुरत नहीं है। स्कूली भोजन में अंडा देने की बात अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निशुल्क दवा देने की बात - बीते दस सालों का एक अदद सबक तो यही है कि सार्वजनिक सेवाओं को सुधारा जा सकता है। लेकिन ये छोटे-छोटे कदम तभी शुरू हो पाते हैं जब यह माना जाए कि गरीब की जिंदगी में सरकारी सामाजिक सहायता का बुनियादी महत्व है। अगर सामाजिक नीतियां विवेक-सम्मत न हुईं तो फिर विकास उर्फ ग्रोथ-मैनिया का भ्रम भी बहुत अधिक लाभदायक नहीं होगा। ये जो पब्लिक है समझती सब है भले ही कुछ देर से समझे।